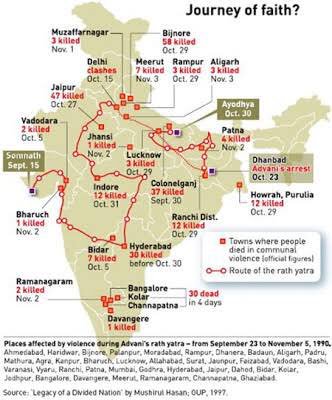अप्रासंगिक Aprasangik
राजनीति क्या सिर्फ रणनीति का खेल है?क्या उससे आदर्श की संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई है?क्या अब हम किसी राजनेता या दल की प्रशंसा सिर्फ इसलिए करने को बाध्य हैं कि उसने कुशल या चतुर रणनीति के जरिए अपने विरोधियों को हक्का बक्का छोड़ दिया है?ये प्रश्न भारत के लिए,खासकर,उसकी राजनीति के सन्दर्भ में प्रासंगिक हो उठे हैं. राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में अलग-अलग राजनीतिक दलों की भूमिका ने हमें इन पर नए सिरे से इन सवालों पर सोचने को मजबूर किया है.भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में जन्मना दलित रामनाथ कोविंद का नाम प्रस्तावित करते ही ऐसा लगा जैसे उसने अपना तुरुप का पत्ता विपक्ष के मुँह पर फ़ेंक दिया है और अब विपक्ष के पास कोई चारा ही नहीं बचा है.रामविलास पासवान ने आगे बढ़कर कह डाला कि जो कोविंद का विरोध करेगा वह दलित विरोधी माना जाएगा.
मीडिया फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस चाल पर, जिसमें विपक्ष के लिए मात ही मात थी, मुग्ध हो उठा. कुछ ऐसी ही हालत उसकी उस वक्त हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व ने अब्दुल कलाम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया था.वरिष्ठ पत्रकार एजाज़ अशरफ ने ठीक ही इसकी याद दिलाई है और दोनों ही निर्णयों के पीछे की रणनीति को समझने को कहा है.
कलाम का नाम 2002 के गुजरात की मुस्लिम विरोधी हिंसा के बाद आया. इस हिंसा के लिए जवाबदेही तय करने में और इन्साफ निश्चित करने वाजपेयी की दिलचस्पी में कोई दृढ़ता न थी.लेकिन यह तथ्य था कि गुजरात की हिंसा चल नहीं सकती थी अगर वहाँ की तत्कालीन सरकार ने या तो उसे शह न दी होती या उसकी ओर से आँख न मूँद ली होती. भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने गुजरात के अपने नेतृत्व को अनुशासित करने के लिए भी कुछ नहीं किया. उसकी छवि पर मुस्लिम विरोधी का जो धब्बा पहले से लगा था,वह और गाढ़ा हो गया. कलाम का नाम इस पृष्ठभूमि में लाया गया था.एजाज़ ठीक कहते हैं कि यह मुसलमानों को सांत्वना देने से कहीं ज़्यादा हिदुओं को अपने भीतर की अपराध ग्रंथि को सहलाने को था :कलाम के चुनाव ने आखिर यह दिखा दिया कि भाजपा को मुसलमान से परहेज नहीं, आखिर वह एक मुसलमान को राष्ट्रपति तक बनाने को तैयार है और गुजरात में जो कुछ हुआ उसे भाजपा का मुस्लिम विरोध नहीं कहा जा सकता.यह एक अलग बात है कि कलाम एक हिंदू दीखते मुसलमान थे. उन्हें देखकर मुझे बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से सुनी यह बात याद आ गई कि मुसलमान “मोहमडन हिंदू” के रूप में उन्हें स्वीकार्य हैं.
कोविंद का नाम उस समय प्रस्तावित किया गया है जब देश में दलित क्षोभ अलग-अलग रूप में जाहिर हो रहा है.इसका कारण खासकर पिछले तीन सालों में दलितों पर बढ़े हमले हैं.दलितों के प्रति इस सरकार का रवैया इससे साफ़ हो गया कि उसने पूरी ताकत यह साबित करने में लगा दी है कि रोहित वेमुला दलित थे ही नहीं. उसके बाद दलितों पर आक्रमण की घटनाएँ बढ़ती चली गई हैं.सरकार के मुखिया की प्रतिक्रिया क्या थी:दलितों को न मारो,भले मुझे मार लो!
कोविंद या उन जैसे किसी दलित का नाम आ सकता है,यह कयास पहले से लगाया जा ही रहा था.यह फिर एक चुस्त चाल है:आप भाजपा को आखिर दलित विरोधी कैसे कह सकते हैं जब वह एक दलित का नाम देश के सर्वोच्च पद के लिए प्रस्तावित कर रही हो! आखिर फली नरीमान जैसे संविधान के जानकार ने भी इसके लिए सरकार को बधाई दे ही डाली और अकादमिक जगत के दलित मुद्दों के विशेषज्ञ भी यह कह रहे हैं कि इस कदम से भाजपा ने खुद को एक सर्वसमाज का दल साबित किया है और विरोधी दलों का यह मुद्दा निष्प्रभावी कर दिया है कि सरकार दलित विरोधी है.
विपक्ष ने इस पर प्रत्याशित प्रतिक्रिया ही की कोविंद के नाम के जवाब में मीरा कुमार का नाम प्रस्तावित करके.उसका यह कदम विश्वसनीय नहीं क्योंकि शह और मात के खेल में खेल में वह पिछड़ गया है. अगर यह वह पहले कर पाता तो फिर भी उसकी चुस्ती दीखती.एक दलित का जवाब एक दलित:इसमें कुछ अश्लीलता है क्योंकि ऐसा लगता है कि लक्ष्य तो कुछ और है,दलित उपलक्ष्य मात्र है.
विपक्ष एक मौक़ा चूक गया:वह संसदीय राजनीति के पहचाने हुए दाँवपेंच में पड़ने से इन्कार करते हुए यह कह सकता था कि राष्ट्रपति का पद उसके लिए आज के दौर में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा से जुड़ा हुआ है और वह इसे सामाजिक न्याय के प्रतीकों के खेल में शेष नहीं करना चाहता. उसके लिए ऐसा नाम चाहिए जिसने इन मूल्यों के पक्ष में इस प्रकार का नैतिक साहस कभी दिखाया हो. गोपाल कृष्ण गांधी का नाम इसलिए उपयुक्त था कि अपनी उदार वाम छवि के बावजूद उन्होंने बंगाल का राज्यपाल रहते हुए सिंगुर और नंदीग्राम की राज्य समर्थित हिंसा की आलोचना की थी और वाम मोर्चा सरकार को संवैधानिक आदर्शों की याद दिलाई थी.लेकिन सुना जाता है कि खुद उन्होंने एक दलित का नाम प्रस्तावित करने का सुझाव दिया. इससे सिर्फ यह पता चलता है कि रणनीति ही अब आदर्श या मूल्य का भ्रम देने लगी है और अच्छे खासे लोग इसके झाँसे में आ सकते हैं.
भारत खुद को आदर्शों का देश कहता रहा है लेकिन अब आदर्श का पक्ष लेना यहाँ दुस्साहस या मूर्खता से अधिक कुछ नहीं. इस समय भारत को उन देशों की ओर देखने की ज़रूरत है जिनकी संस्कृति को पाश्चात्य कहकर उन्हें हीन मानने की उसे आदत पड़ चुकी है.हाल में ब्रिटेन में हुए चुनाव में जेरेमी कोर्बिन ने न सिर्फ आर्थिक मसलों पर, बल्कि सामाजिक प्रश्नों पर भी वह रुख लिया जिसे इस समय दुस्साहसी कहा जाएगा.उनके पहले फ्रांस में मैक्रन ने भी स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद का विरोध किया था और जर्मनी में भी राज्य के नेतृत्व ने अलोकप्रियता का खतरा उठाकर शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोलने का ऐलान किया था. ये राजनेता डरे नहीं,उन्होंने जनता को झाँसा देने की कोशिश नहीं की, उनसे स्पष्ट रूप से आदर्शों के संघर्ष में अपना पक्ष चुनने को कहा.यह साहस भारत के राजनीतिक नेतृत्व में नहीं है,फिर भी वह जाने क्यों खुद को किसी कल्पित महान संस्कृति का वारिस बताता है.
- सत्याग्रह, जून, 2017
- https://satyagrah.scroll.in/article/107863/is-politics-just-a-game-of-manipulation