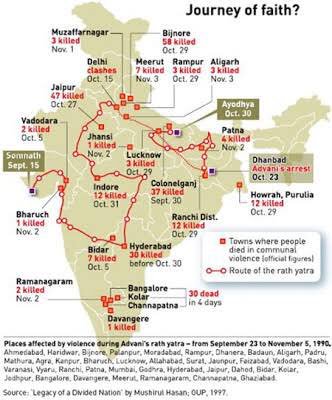अप्रासंगिक Aprasangik
अयूब पंडित की हत्या (Ayub Pandit’s mob lynching)
प्रत्येक आन्दोलन के सामने ऐसे क्षण आते हैं जब उसे ठहरकर अपने बारे में कुछ नया फैसला करना पड़ता है. जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के सामने अभी ऐसा ही एक मौक़ा है. मौक़ा एक तकलीफदेह वारदात से पैदा हुआ है : कल रात श्रीनगर में नौहट्टा की जामा मस्जिद के पास तैनात पुलिस अधिकारी अयूब पंडित की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर डाली. यह भीड़ उन लोगों की थी जो मस्जिद और उसके शबे कद्र (बरकत की रात) मनाने इकट्ठा हुए थे. कहा जाता है कि अयूब मस्जिद की गिर्द तस्वीरें ले रहे थे जिस पर भीड़ को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें घेरकर पीटना शुरू कर दिया, उनके कपड़े फाड़ डाले. उन्होंने, बताया जाता है आत्मरक्षा में अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोलियां चलाईं जिससे भीड़ और भड़क उठी और फिर पीट पीट कर उनका क़त्ल कर दिया.पूरे घटनाक्रम के बारे में शायद ही हमें ठीक ठीक कुछ मालूम हो सके. लेकिन यह तय है कि भीड़ ने अयूब की हत्या की.
अयूब पुलिस अधिकारी थे. उनका यह काम था किसी अप्रिय, हिंसक घटना को रोकने की कोशिश करना. अगर वे तस्वीर ले रहे थे तो यह उनके काम में शामिल था.
आम तौर पर कश्मीर की चर्चा पत्थरबाजी पर केन्द्रित रहती है. जो पत्थरबाजी में शामिल हैं, कहा जाता है कि वे अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां आते हैं. वे इसके जरिए अपनी तरफ से भारतीय शासन का विरोध कर रहे हैं. इसकी कीमत है जो कभी वे पेलेट गन से आंख गँवा कर और कभी जान देकर चुकाते रहे हैं. हम सबने पेलेट गन का विरोध किया है.
राज्य की हिंसा की हम सब मुखालफ़त करते रहे हैं. लेकिन क्या भारतीय राज्य के विरोध की हिंसा जायज़ है?
अयूब पंडित की मौत या उनके क़त्ल ने यह मौक़ा कश्मीर की जनता को दिया है और उनके नेतृत्व को भी: कि वे रुक जाएं और अपने तरीके के बारे में विचार करें. यह इसलिए कि कल की घटना में कुछ परेशानकुन इशारे हैं: अयूब किसी ऐसे हमले में शामिल नहीं थे जो पुलिस जनता पर कर रही थी, वे किसी मुठभेड़ के बीच नहीं थे. यह भीड़ हथियारबंद भी नहीं थी. उसने अयूब को घेरा और वे उस वक्त अकेले थे. अयूब की हत्या उसी तरह की गई जैसे पहेलू खान की या अख़लाक की की गई थी. जिसमें भीड़ को मालूम था कि हर कोई जो अगल-बगल है, इस कृत्य में शामिल है और इसका समर्थक है. हालाँकि अयूब के पास पिस्तौल थी, लेकिन वह उस भीड़ के आगे बेकार थी यह भीड़ को मालूम था.
कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में अगर हिंसा या तशद्दुद लाज़िमी तौर पर शामिल हो, भले ही भारतीय राज्य की हिंसा के जवाब में तो वह तहरीक अपनी पाकीज़गी खो देती है.
अब तक हम दहशतगर्दों और कश्मीरी जनता के प्रतिरोध में अंतर करते आए हैं. लेकिन यह साफ़ है कि कश्मीर के आन्दोलन को अहिंसक रखना कठिन है. यह भी कि कश्मीर के नेतृत्व में खुद यह नैतिक क्षमता नहीं वे कि वे यह कह सकें कि चाहे जितनी कुर्बानी देनी हो, हमारी ओर से हिंसा न होगी.
अयूब की हत्या एक चेतावनी की तरह देखी जानी चाहिए: हिंसा जब इस तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए और आज़ादी जैसी एक भावना को बनाए रखने के लिए अनिवार्य उत्तेजक ड्रग बन जाए तो उस समाज में कोई भी विवेकपूर्ण निर्णय करना असंभव हो जाएगा.
यही कारण था कि गांधी ने चौरी चौरा में आन्दोलनकारियों के द्वारा पुलिसवालों को मार दिए जाने के बाद राष्ट्रव्यापी आन्दोलन वापस ले लिया था. नेहरू जैसे उनके अनुयायी भी इस निर्णय से हैरान हुए थे. कुछ का मानना था कि यह गाँधी का नैतिक नहीं रणनीतिक फैसला था. चूँकि आन्दोलन पहले ही कमजोर हो रहा था, उन्हें उसे जारी न रखने का एक बहाना मिल गया. लेकिन गाँधी के लिए यह सैद्धांतिक मसला था: क्या स्वाधीनता आन्दोलन का साधन हिंसक होगा? फिर उस साधन से प्राप्त स्वतंत्रता कैसी होगी?
चौरी चौरा से नौहट्टा की तुलना शायद गलत है. दोनों वक्त भी संभवतः तुलनीय नहीं हैं. लेकिन फिर भी यह सवाल बना रहता है कि क्या आज़ादी जैसी संवेदना की पवित्रता को यह खूँरेजी पूरी तरह खत्म नहीं कर देती?
पिछले दिनों हमने पत्थरबाजी को लेकर कई तरह की बहसें सुनी हैं. वह एक जश्न की तरह होता जा रहा है और एक रूटीन की तरह. जान जाना भी रूटीन है. कहा जाता है कि इसे भारी जन समर्थन हासिल है. लेकिन यह जनसमर्थन कोई नई चीज़ नहीं. हर प्रकार की हिंसा को किसी न किसी तरह का जन समर्थन हासिल रहता ही है: प्रायः उन सब कायरों का जो खुद को खतरे में नहीं डालना चाहते, लेकिन अपनी ओर से हत्या ज़रूर चाहते हैं. मगर हिंसा जब आदत बन जाती है तो समाज में एक विकृति आ जाती है. क्या हम यह सोचते हैं कि इस हिंसा का कारण खत्म हो जाने पर यह हिंसा भी खत्म हो जाएगी? यह विचार एकदम गलत है.
मैक्सिम गोर्की ने इसी वजह से बोल्शेविक क्रान्ति के बाद लेनिन की आलोचना की थी. उनका लेनिन पर आरोप था कि वे साधारण रूसी जनता को हिंसक और कातिल बना रहे हैं: वे वर्ग शत्रुओं के संहार के नाम पर भीड़ के इन्साफ को बढ़ावा दे रहे हैं और यह अपराध है.
कभी भी देर नहीं होती. अयूब पंडित की मौत का सोग सिर्फ राज्य मनाए, सिर्फ पुलिस उस पर शोक प्रकट करे और कश्मीर की आज़ादी पसंद तहरीक इस पर एक मिनट खामोश भी न हो सके, उसके पास अफ़सोस के दो लफ्ज़ भी न हों तो मानना चाहिए कि कहीं कोई भारी दुर्घटना इस सामाजिक अवचेतन के साथ घट चुकी है और उससे उबरने के लिए उसे बड़े नैतिक साहस की ज़रूरत है.
मौके मिलते हैं और किसी समाज की पहचान इससे होती है कि वह उनके साथ कैसे पेश आता है. कश्मीर की जनता के लिए एक ऐसी ही घड़ी आ खड़ी हुई है. कदम पीछे खींचना, अपनी आलोचना करना कई बार अधिक बड़ी बहादुरी है. कश्मीर यहाँ उदाहरण पेश कर सकता है.
- बीबीसी हिंदी डॉटकॉम, जून, 2017
- http://www.bbc.com/hindi/india-40388031